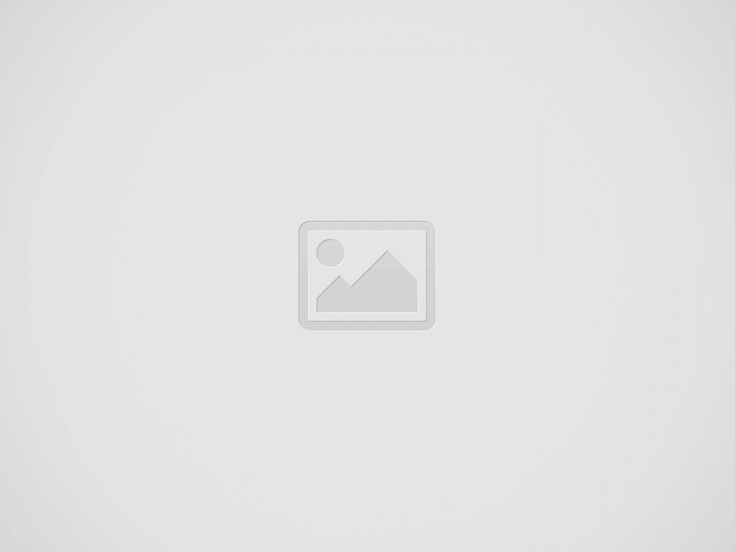

सूक्ष्मजीव लगभग हर जगह अपने उच्च अनुकूलन क्षमता के कारण मौजूद हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक उन लोगों की तलाश में हैं जो कठोर परिस्थितियों में बढ़ सकते हैं। इस तरह के रोगाणुओं को अद्वितीय प्रोटीन और लिपिड को संश्लेषित करने में मदद मिल सकती है जिसमें कई अनुप्रयोग हो सकते हैं।
6 जून 2017 को, राजस्थान के मुकुंदपुर गांव में एक उल्का एक रेतीले कृषि क्षेत्र पर उतरा। एक शोध दल ने बैक्टीरिया को अलग करने और प्रभाव स्थल पर अध्ययन करने के अवसर को जब्त करने का फैसला किया क्योंकि वे उल्कापिंड के प्रभाव से उत्पन्न उच्च दबाव और तापमान को पीछे छोड़ देंगे। उल्कापिंड अत्यधिक घने सामग्री (2300 किलोग्राम / घन मीटर) से बना था और इसका वजन 2.26 किलोग्राम था। यह लगभग 11 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के अनुमानित वेग से यात्रा कर रहा था। जमीन से टकराने पर, इसने 43 सेमी व्यास और 15 सेमी गहराई में एक गोलाकार गड्ढा बनाया।
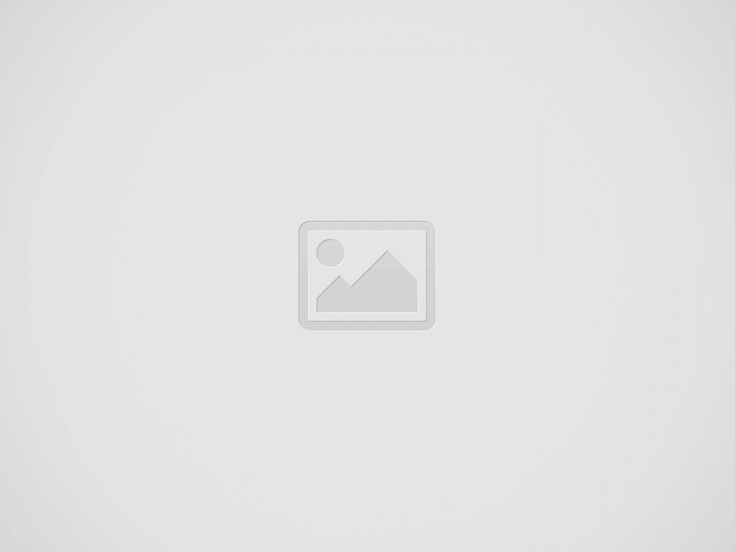

भारतीय शोधकर्ता गर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाते हैं जो उल्कापिंड के प्रभाव से बचे हैं
पुणे स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की एक शोध टीम ने घटना के 48 घंटे के भीतर, उल्कापिंड से प्रभावित नहीं होने वाले आस-पास के क्षेत्रों के नमूनों के साथ, प्रभाव के स्थान से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र किए। प्रयोगशाला में, मिट्टी के नमूनों को पहले पोषक तत्व से युक्त मध्यम परिवेश में और बाद में 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जोड़ा जाता था। एक बार जब बैक्टीरिया पर्याप्त संख्या में बढ़ गए, तो उनके डीएनए को जीन 16S rRNA के एक छोटे टुकड़े के लिए निकाला और सिल दिया गया। इसने शोधकर्ताओं को बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद की, जो रोगाणुओं के ऑनलाइन डेटाबेस से जानकारी का उपयोग करते हैं। आगे के विश्लेषण से पता चला कि गैर-प्रभाव वाले क्षेत्रों की तुलना में प्रभावित क्षेत्र के नमूनों में दो बैक्टीरिया, बेसिलस थर्मोकॉप्रिया IR-1 और ब्रेविबैसिलस बोरस्टेनलेन्स अधिक प्रमुख थे। बैसिलस थर्मोकॉप्रिया आईआर -1 का अधिक बारीकी से अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि यह 60 डिग्री और 10 प्रतिशत नमक के घोल के तापमान पर बढ़ने में सक्षम था। यह प्रयोगशाला में सिम्युलेटेड स्थिति जैसी उल्कापिंड के प्रभाव से भी बच सकता है।
“ताजा गिरावट वाली जगहों पर माइक्रोबियल विविधता पर उल्कापिंड के प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसे दबावों के तहत जीवित रहने वाले रोगाणुओं की पहचान, अंतरिक्ष से संबंधित तनाव और अंतःविषय यात्रा के प्रभावों के अध्ययन में मदद कर सकती है, ”डॉ रेबेका एस। थॉम्ब्रे ने समझाया, जिन्होंने मॉडर्न कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की शोध टीम का नेतृत्व किया था इंडिया साइंस वायर से बात की। डॉ। थॉम्ब्रे के अलावा, टीम में पी.पी. कुलकर्णी, ई। शिवकार्तिक, टी। पाटस्कर, बी.एस. पाटिल (मॉडर्न कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, पुणे); भालमुरुगन शिवरामन, जे.के. मीका, और एस। विजयन (भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद); पराग ए। वैशम्पायन और अरमान सेइलेमेज़ियन (कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए)। अध्ययन के निष्कर्षों को जर्नल एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन को इसरो-स्पेस टेक्नोलॉजी सेल, पुणे द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
Is this the replacement remote that will elevate your AC experience? Tired of struggling with…
Is this the air quality monitor that every health-conscious individual needs? Are you concerned about…
Is this the ultimate air conditioner for tech enthusiasts? Did you know that a good…
Is Your AC Ready to Chill in 2025? Discover the Smart Thermostat Revolution! Let’s face…
Introduction to Cool Comfort Are you sweating it out in the unbearable heat of the…
Unpacking the hype: Can this mini cooler really keep you cool? Feeling the heat but…